उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन और संघर्ष उत्तराखंड राज्य का निर्माण कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह दशकों लंबे संघर्ष, बलिदान और जन-आंदोलन का परिणाम था । हालांकि अलग राज्य की मांग 1897 से ही समय-समय पर उठती रही थी, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया । जब आप उत्तराखंड का आंदोलन ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे तो आपको आभास होगा जिस प्रकार भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाई ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य को बनाने में संघर्ष हुए। यह बात तो सच है की उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर में बांध बनाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किए। न सड़कें बनवायी न ही पर्यटन में विकास किया और बिजली तो पहाड़ों में दूर दूर तक नहीं पहुंची । जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश काफी आगे बढ़ गया। तो जरूरत तो थी एक नये राज्य की इसलिए तो संघर्ष हुआ। आप जब उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ें तो स्वतंत्र भारत आंदोलन से तुलना करें। जैसे भारत आजाद करने की प्रथम लड़ाई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वैसे ही उत्तराखंड की प्रथम लड़ाई 1947 से तुलना करें। ये बात अलग है कि भारत का वह संग्राम असफल हुआ औ...
भारतीय संविधान
भारत की न्यायालय व्यवस्था
भारतीय संविधान के भाग -5 (अनुच्छेद 124 से 147 तक)
भारतीय न्यायालय व्यवस्था का इतिहास
भारत में सबसे पहले 1773 का 'रेग्यूलेटिंग एक्ट' के द्वारा 'कलकत्ता' में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
जिसका क्षेत्राधिकार बिहार व उड़ीसा तक विस्तृत था। इससे बाहर के मामलों में दोनों पक्षों की सहमति और कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के अनुमति से सुनवाई हो सकती थी।
भारत सरकार अधिनियम 1935
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक संघीय न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है ।
आजादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा भारत में तीन स्तरीय एकीकृत न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया।
संविधान लागू होने के पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय का आयोजन संसद भवन के 'चेंबर ऑफ प्रिंसेस' में किया जाता था। वर्तमान परिसर में इसका आयोजन 1958 से हो रहा है।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या
प्रारंभिक समय में संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1956 में संसद ने अन्य न्यायाधीशों की संख्या 10 निश्चित की। 1960 में 13, 1977 में 17, और 1986 में 25।
प्रारंभ में - 8 थी
- 1956 में — 11
- 1960 में — 14
- 1977 में — 18
- 1986 में — 26
- 2009 में — 31
- 2019 में — 35
संविधान लागू होने के बाद से अब तक 6 बार बढायी गयी है।
भारत का सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 124)
'भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा'।
जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा उतने न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। जितने की समय-समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे।
प्रश्न 01 - न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है?
उत्तर - राष्ट्रपति
प्रश्न 02 - न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है?
उत्तर - संसद
(वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 35 है और यह नई दिल्ली में स्थित है। परंतु मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसका आयोजन भारत में कहीं भी कर सकता है।)
प्रश्न 01 - भारत के वर्तमान एवं 50 वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
उत्तर - डीवाई चंद्रचूड़
न्यायधीश बनने के लिए योग्यता
- भारत का नागरिक हो।
- एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो।
- एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो।
- राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।
नियुक्ति :- राष्ट्रपति द्वारा
सर्वोच्च न्यायधीश का कार्यकाल
- 65 वर्ष की आयु
- इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर छोड़ सकता है
- साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं।
न्यायालय का क्षेत्राधिकार
- प्रारंभिक (मूल क्षेत्राधिकार) (अनुच्छेद 131)
- अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132-134)
- सलाहकार क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 143)
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 131)
इस अनुच्छेद का प्रयोग राजनीतिक भावना से प्रेरित विवादों के निपटारे के लिये नहीं किया जा सकता। बल्कि केंद्र सरकार और राज्यों के बीच के विवादों को सुलझाया जाता है।
अपीलीय क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 132 - 134)
जब किसी निम्न न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई उच्च न्यायालय में होती है तो इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपील करने का न्यायालय है। अर्थात हम कह सकते हैं कि निचले स्तर के न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सिविल और फौजदारी मामले उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण-पत्र अनुच्छेद 134ए के तहत दे दिया है कि उक्त मामले में संविधान विधि का प्रश्न अंतरहित हो और उच्च न्यायालय अपील का प्रमाण पत्र दे।
विशेष इजाजत से अपील (अनुच्छेद 136)
सैन्य न्यायालय के निर्णय को छोड़कर अन्य किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय अपील की विशेष इजाजत प्रदान कर सकता है।
न्यायिक पुनर्विलोकन (अनुच्छेद 137)
उच्चतम न्यायालय पश्चावर्ती (बाद में जाने वाले) मामलों में अपने पूर्व निर्णय को रद्द या परिवर्तित कर सकता है।
अनुच्छेद 139 मूल अधिकारों के उल्लंघन के उल्लघंन पर उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी कर सकता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेरा
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा
संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद -32)
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक "Right to consitutional remedies" - में अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान की आत्मा" (heart and soul of the consitution) कहा है।
सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय 5 रिट जारी करते हैं।
रिट का अर्थ होता है - 'आज्ञापत्र' या 'writ' । साधारण शब्दों में कह तो एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का आदेश ।
बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas Carpurse - शरीर लेकर आओ)
यह आदेश अनुचित (गैर कानूनी) गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। और 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत यदि किसी व्यक्ति को किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है।
परम + आदेश (परमादेश) (madamos)
यह एक न्यायिक उपचार है। परमादेश का अर्थ होता है - "हमारा आदेश है कि"। यह सरकारी पद पर कार्यरत अधिकारियो, मंत्रियों, निचली, अदालतों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह उस समय दिया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने पद से जुड़े हुए कार्य को ठीक से नहीं करता है तब परमादेश रिट जारी करके उसको अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्यों को करने का आदेश दिया जाता है।
प्रतिषेध (prohibition)
प्रतिषेध का अर्थ होता है - रोक देना।
इस आदेश द्वारा ऊपरी अदालत निचली अदालत को यह आदेश देता है कि वह संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध चल रही न्यायिक कार्यवाही को रोक दें।
उत्प्रेषण (Certiorari)
उत्प्रेषण का अर्थ है - सूचित करने के लिए
यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की कार्रवाई को अपने पास मंगवा कर कार्यवाही करने के आदेश को सूचित करती है।
अधिकार पृच्छा (Quo warranto)
अधिकार पृच्छा का अर्थ है - "किस वारंट द्वारा"
सरकारी कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच के लिए कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है। जिसका वह हकदार नहीं है। अर्थात कोई गलत तरीके से सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है।
उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214 से 231 तक)
भारत में उच्च न्यायालय का सर्वप्रथम गठन 1862 में हुआ।
1862 में सबसे पहले कोलकाता में उच्च न्यायालय की हुई फिर मद्रास और बंबई में हुई। सन् 1866 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय की हुई।
1956 में 7वें संविधान संशोधन किया गया । और संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। भारत देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। राज्य में 24 उच्च न्यायालय व 25वां केवल दिल्ली ऐसा केन्द्रीय शासित प्रदेश है। जिसका अपना उच्च न्यायालय है। जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
पंजाब - हरियाणा दोनों राज्यों का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है।
उच्च न्यायालय (अनुच्छेद 214)
प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। जो एक मुख्य न्यायाधीश एवं उतने अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा । जितने की समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करना आवश्यक समझे।
योग्यता
- भारत का नागरिक हो।
- भारत में कहीं भी लगातार 10 वर्षों से न्यायिक कार्य।
- HC या न्यायालयों में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।
न्यायाधीशों की नियुक्ति (अनुच्छेद 217)
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी।
- शपथ राज्यपाल द्वारा दी जाती है
कार्यकाल
- संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है लेकिन अधिकतम आयु 62 वर्ष तक पद में रह सकता है।
- इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है।
- संसद की सिफारिश राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है।
- साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर संसद।
- यदि नियुक्ति SC में हो जाए तो पद छोड़ सकता है।
न्यायाधीशों को हटाना
- 100 सदस्यों (लोकसभा) अथवा 50 (राज्यसभा) के सदस्यों के हस्ताक्षरित हटाने का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष व राज्य सभा के सभापति सभापति को सौंपना होगा।
- अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकृति और अस्वीकृत कर सकता है।
- यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो आरोपों को जांच के लिए 3 संसदीय समिति गठित किया जाएगा। समिति में SC का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रख्यात न्यायविद होने चाहिए।
- यदि समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार दोषी है यह आयोग्य है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
- दोनों सदनों से विशेष बहुमत 2/3 प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के आदेश से नागरिकों को हटा दिया जाता है।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (अनुच्छेद 223)
- राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या।
- उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश स्थायी रूप से अनुपस्थित हो।
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 225)
1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
- संसद सदस्यों और राज्य विधान मंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा
- जिला पंचायत व नगर पंचायत के अध्यक्षों के निर्वाचन से संबंधित विवादों को सुलझाता है ।
- राजस्व मामले नागरिकों को मूल अधिकारों का परिवर्तन
- वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून व न्यायालय की अवमानना।
2. रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 226)
उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अलग ना होकर उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 32 के समवर्ती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का शोषण होता है तो पीड़ित व्यक्ति का अधिकार है कि वह यादव उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकता है।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण
- परमादेश
- प्रतिषेध
- उत्प्रेषण
- अधिकार पृच्छा
3. अपीलीय क्षेत्राधिकार
उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है यहां इसके राज्य क्षेत्र के तहत आने वाले अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। यहां जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील का प्रमाण पत्र होने पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
4. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार
उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्र के सभी न्यायालय व सहायक न्यायालय के क्रियाकलापों पर नजर रखें।
5. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
उच्च न्यायालय के अपीलीय न्यायिक क्षेत्र एवं न्यायिक शक्तियों के साथ प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति के प्रस्ताव, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण करता है।
6. अभिलेख न्यायालय
उच्च न्यायालय के सभी फैसले कार्यवाही और कार्य अभिलेखों के रूप में सुरक्षित साक्ष्य के तौर पर रखे जाते हैं। अभिलेख न्यायालय के रूप में एक उच्च न्यायालय किसी मामले के संबंध में दिए गए अपने स्वयं के आदेश अथवा निर्णय की समीक्षा कर सकता है और उसमें सुधार की शक्ति भी उसे प्राप्त है। हालांकि इस संबंध में संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को कोई विशेष शक्ति प्रदान नहीं की गई है वहीं दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय को संविधान में विशिष्ट रूप से अपने निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान की है।
7. न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति
उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल का केंद्र सरकार दोनों के अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की वैधानिकता के परीक्षण के लिए है।
जिला एवं सत्र न्यायालय (अनुच्छेद 233 से 237 तक - भाग VI)
प्रत्येक जिले का एक न्यायालय होगा। जब वह सिविल मामलों की सुनवाई करेगा तो वह 'जिला न्यायालय' कहलाएगा।
जब आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा तो वह जिला सत्र न्यायालय कहलाएगा।
जिला न्यायाधीश की नियुक्ति (अनुच्छेद 233)
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं पदों में उन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के सलाह से की जाती है। जिसके लिए निम्न योग्यताएं आवश्यक है -
- कोई भी व्यक्ति जिसमे अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो।
- लाभ के पद पर न हो।
- उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण (अनुच्छेद 235)
जिला न्यायाधीश न्यायिक शक्तियों के साथ प्रशासनिक शक्तियां भी प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय जिला न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति के प्रस्ताव, पदोन्नति एवं अन्य मामलों पर नियंत्रण करता है।

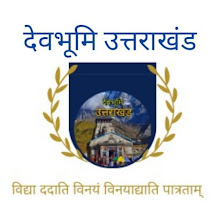

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts.
Please let me now.