उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन और संघर्ष उत्तराखंड राज्य का निर्माण कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि यह दशकों लंबे संघर्ष, बलिदान और जन-आंदोलन का परिणाम था । हालांकि अलग राज्य की मांग 1897 से ही समय-समय पर उठती रही थी, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद इस संघर्ष ने एक नया मोड़ लिया । जब आप उत्तराखंड का आंदोलन ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे तो आपको आभास होगा जिस प्रकार भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाई ठीक उसी प्रकार उत्तराखंड राज्य को बनाने में संघर्ष हुए। यह बात तो सच है की उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर में बांध बनाने के अलावा कोई भी कार्य नहीं किए। न सड़कें बनवायी न ही पर्यटन में विकास किया और बिजली तो पहाड़ों में दूर दूर तक नहीं पहुंची । जबकि दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश काफी आगे बढ़ गया। तो जरूरत तो थी एक नये राज्य की इसलिए तो संघर्ष हुआ। आप जब उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के बारे में पढ़ें तो स्वतंत्र भारत आंदोलन से तुलना करें। जैसे भारत आजाद करने की प्रथम लड़ाई 1857 का स्वतंत्रता संग्राम वैसे ही उत्तराखंड की प्रथम लड़ाई 1947 से तुलना करें। ये बात अलग है कि भारत का वह संग्राम असफल हुआ औ...
भारतीय संविधान
भारत का राष्ट्रपति एवं मंत्रिमंडल (भाग - V)
संघ की कार्यपालिका शक्ति (केन्द्र सरकार)
(1). राष्ट्रपति (अनुच्छेद 52)
(2). उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63)
(3). मंत्री परिषद (अनुच्छेद 74)
(4). महान्यायवादी (अनुच्छेद 76)
(5). CAG (अनुच्छेद 148)
भारत का राष्ट्रपति
वर्तमान राष्ट्रपति (2022) - श्रीमति द्रौपदी मुर्मू (15 वीं राष्ट्रपति)
प्रथम राष्ट्रपति - डां. राजेन्द्र प्रसाद
अनुच्छेद 52 - भारत का एक राष्ट्रपति होगा।
अनुच्छेद 53 - संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
राष्ट्रपति का निर्वाचन - (अनुच्छेद 54)
(1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
(2) राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा
(दिल्ली व पांडिचेरी भी शामिल)
(3) अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा - अप्रत्यक्ष विधि से
राष्ट्रपति का कार्यकाल - (अनुच्छेद 56)
(1) शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष
(2) इससे पहले उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है।
(3) संविधान उल्लघंन पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है।
पुनः निर्वाचन - (अनुच्छेद 57)
6 माह के अंदर
राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता - (अनुच्छेद 58)
(1) भारत का नागरिक हो
(2) 35 वर्ष की आयु हो
(3) लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो
(4) लाभ के पद पर न हो
*लाभ का पद क्या है ?
संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संसद सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए 'लाभ का पद' शब्द का प्रयोग किया गया है परंतु संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने इसकी व्याख्या में कहा- कोई व्यक्ति जो सरकार के अधीन किसी कर्तव्य का निर्वहन करता है करता है और बदले में उसे वेतन, फीस, कमीशन या अन्य कोई सुविधा प्राप्त होती है तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाएगा और उसका पद लाभ का पद माना जाएगा परंतु संसद बीड़ी बनाकर ऐसे किसी भी पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है।
राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां
(1) विधायी कार्य
(2) प्रशासनिक कार्य
(3) न्यायिक कार्य
विधायी कार्य :-
(1) राष्ट्रपति संसद का अंग होता है
(2) बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता है।
(3) राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सत्र को आहूत/सत्रावासन करता है। (आहूत का अर्थ है - निमंत्रित करना या बुलाना)
राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्तियां (vito power)
(1) संपूर्ण निषेधाधिकार
संसद से विधेयक पारित होने के बाद संपूर्ण निषेधाधिकार के तहत राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो विधेयक पूर्ण समाप्त हो जाता है।
(2) निलंबनकारी निषेधाधिकार
संसद से विधेयक पारित होने के बाद निलंबनकारी निषेधाधिकारी के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस संसद में भेज सकता है किन्तु संसद के विधेयक पर पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होता है। (*क्योंकि इस प्रक्रिया में विधेयक कानून बनने से कुछ समय के लिए रुक जाता है जिसे निलंबनकारी विशेषाधिकार कहा जाता है)
(3) जेबी निषेधाधिकार
संसद से पारित विधेयक को राष्ट्रपति जेबी निषेधाधिकार के तहत ना तो हस्ताक्षर करता है। और ना पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। अर्थात अनिश्चितकाल के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है।
नोट :- 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति 'ज्ञानी जैल सिंह' ने डाक संशोधन विधेयक (1986) पर 'जेबी वीटो का प्रयोग किया
अध्यादेश जारी करना (अनुच्छेद - 123)
यदि संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो और कोई कानून तत्काल लागू करने की आवश्यकता हो, तो कुल विषयों तक, जहां तक संसद को कानून बनाने का अधिकार है। वह यह कि राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से कोई कानून लागू कर सकता है। किंतु अध्यादेश जारी करने के पश्चात बैठक से 6 सप्ताह के भीतर संसद की सहमति प्राप्त करनी होता है।
दो सत्र के मध्य अधिकतम छह माह तक अंतराल हो सकता है इसलिए अध्यादेश की अधिकतम अवधि (6 माह + 6 सप्ताह) अथवा 7.5 माह हो सकती है।
राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्य
(1) संघ की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है।
(2) समस्त अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियों पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होते हैं।
(3) अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।
(4) संघ स्तर के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति-
(i) महान्यायवादी
(ii) CAG
(iii) सर्वोच्च न्यायालयका मुख्य न्यायाधीश
(iv) UPSC- अध्यक्ष
(v) निर्वाचन आयोग
(vi) वित्त आयोग
(vii) राष्ट्रीय स्तर के अन्य उपयोग
(viii) तीनों सेनाओं का अध्यक्ष
(ix) विदेश में भारत के राजदूत व उच्च आयुक्त
(x) केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों
(xi) राज्य के राज्यपाल
(xii) प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद आदि की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां
क्षमादान - (अनुच्छेद 72)
राष्ट्रपति किसी भी दंड को क्षमा, परिहार, लघुकरण, निलंबित कर सकता है। (परिहार का अर्थ है - छोड़ना)
सलाहकारी शक्तियां - (अनुच्छेद 143)
सलाहकारी शक्तिया किसी भी विधि या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति व सुप्रीम कोर्ट के लिए सलाह की कोई बाध्यता नहीं है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग - (अनुच्छेद 61)
(1) संसद के किसी भी सदन में उसके कम - से - कम 1/4 सदस्यों द्वारा संविधान उल्लंघन का आरोप लगाया जाएगा
(2) 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं होगी ।
(3) यदि उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन से भेजा जाएगा।
(4) दूसरे सदन में राष्ट्रपति को सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा ।
भारत का उपराष्ट्रपति
वर्तमान उपराष्ट्रपति (2022) - श्री जगदीप धनखड़
प्रथम उपराष्ट्रपति - डां. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
अनुच्छेद 63
भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा ।
अनुच्छेद 64
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा।
उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता - (अनुच्छेद 66)
(1) भारत का नागरिक हो।
(2) 35 वर्ष की आयु हो।
(3) राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो।
(4) लाभ के पद पर न हो।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
(1) संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा ।
(2) अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल
(1) शपथ ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष।
(2) इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है।
(3) संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है
(4) प्रस्तुत प्रस्ताव का प्रारम्भ राज्यसभा में होना अनिवार्य है।
कार्य/शक्तियाॅं
(1) राज्यों का संचालन।
(2) राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा।
(3) उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है।
(4) जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता है तो उसे सभी विशेषाधिकार (उपलब्धियों और भत्ते) राष्ट्रपति के रूप में ही प्राप्त होता है न कि राज्यसभा के सभापति के रूप में।
यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायधीश और वह भी अनुपस्थित हो तो वरिष्ठ न्यायधीश राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेगा।
(5) उपराष्ट्रपति - राष्ट्रपति - राज्यसभा का संचालन - उपसभापति
(6) राष्ट्रपति उपस्थित है या नहीं इसका निर्णय स्वयं राष्ट्रपति करेगा।
(7) 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक,
(8) भारत का राष्ट्रपति जब कभी त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा तक देता है।
(9) दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है।
मंत्रीपरिषद (अनुच्छेद - 74)
राष्ट्रपति की सहायताव सलाह देने के लिए मंत्रीपरिषद का गठन किया जाता है जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करता है। ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति एक बार वापस कर सकता है किंतु दोबारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होता है।
मंत्री परिषद का गठन (अनुच्छेद - 75)
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं।
मंत्री पद की योग्यता
(1) कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है। मंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है, और यदि वह सदस्य नहीं है तो मंत्री पद ग्रहण करने के पश्चात "6 माह के भीतर उसे सदस्यता लेनी होगी" अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं रहेगा।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई है और व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदाई है।
Note :- *सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जो संसद/ विधानमण्डल का सदस्य नहीं है एक लोकसभा/ विधानसभा के कार्यकाल में सिर्फ एक बार ही मंत्री बन सकता है दोबारा मंत्री बनने के लिए उसे सदस्या लेनी होगी।
मंत्रीपरिषद की संरचना
91 वाॅं संविधान संशोधन 2003 में हुआ। जिसके तहत
अनुच्छेद 75 में खण्ड (1) के बाद दो नये खण्ड (खण्ड (क)) और (खण्ड (ख)) जोड़े गये।
खण्ड 1 (क) :- प्रधानमंत्री सहित लोकसभा में मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। वर्तमान समय में कुल लोकसभा सीट 545 हैं। अर्थात मंत्रियों की संख्या 81 से अधिक नहीं होगी। संविधान द्वारा सदन की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है भारत के 1949 के संविधान का अनुच्छेद 81 लोकसभा में संसद के अधिकतम 52 सदस्यों को निर्दिष्ट करता है।
खण्ड (ख) :- संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दल-बदल के आधार पर संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा।
यदि कोई मंत्री 6 महीने निरंतर अनुपस्थित रहता है तो उसका मंत्री पद समाप्त कर दिया जाता है।
मंत्रिमंडल
(1) कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री सहित)
(2) राज्यमंत्री
(3) उपमंत्री
(4) राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(5) संसदीय सचिव
- कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री सहित) - इनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे - ग्रह, रक्षा, वित्त, विदेश एवं अन्य मंत्रालय । (*सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के लिए मात्र कैबिनेट स्तर को मंत्रियों की बैठक बुलायी जाती है)
- राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - यह कैबिनेट मंत्री के सहयोग होते हैं।
- उपमंत्री व स्वतंत्र प्रभार मंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री की प्रशासनिक, राजनीतिक एवं संसदीय सहायता करते हैं।
- संसदीय सचिव मंत्री प्रसिद्ध की अंतिम श्रेणी होती है। इनके पास कोई विभाग या वरिष्ठ मंत्रियों के साथ उनके कार्य में सहायता देने के लिए किया जाता है।
प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य (अनुच्छेद 78)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद -78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति संघ के प्रशासन व कार्यकलाप की जानकारी मांगे तो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए । यदि किसी मंत्री ने अपने विभाग से संबंधित किसी विषय पर कोई निर्णय लिया है जिसे मंत्री परस के विचार के लिए नहीं रखा गया है तो राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री उसे विचार के लिए रखें।
भारत का महान्यायवादी (अनुच्छेद -76)
भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत विधिक मामलों की सलाह एवं सहायता के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रथम महान्यायवादी एम.सी. सीतलवाड़ थे। भारत के वर्तमान व 16वें महान्यायवादी आर. वेंकटरमणि है।
योग्यता
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों बनने की योग्यता
- भारत का नागरिक हो
- उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो।
- राष्ट्रपति के निगाह में न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।
कार्यकाल
- राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्यकाल
- त्यागपत्र — राष्ट्रपति
- पारिश्रमिक निश्चित नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।
कार्य व शक्तियां
- संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं
- मतदान का अधिकार नहीं होता है
- भारत राज्य क्षेत्र के भीतर उसे किसी भी न्यायालय में सुनवाई में हिस्सा लेने का अधिकार होता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद -148)
- नियुक्ति - राष्ट्रपति
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। जिसका मुख्य कार्य संघ एवं राज्य सरकार के व्ययों का लेखा जोखा की रिपोर्ट राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को प्रस्तुत करना है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है यह लोग वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की संपूर्ण व्यवस्था का भी नियंत्रित होता है। CAG का वेतन संसद द्वारा निर्धारित होता है। इसे "साबित कदाचार के आधार" पर पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा CAG सेवानिवृत्त होने के पश्चात संघ एवं राज्य के कोई भी पद धारण नहीं कर सकता।

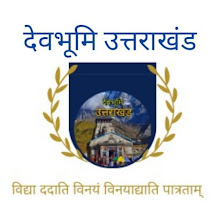

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts.
Please let me now.