भारतीय संविधान
संसद का गठन
संसद क्या है ?
संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख किया गया है कि भारत की एक संसद होगी। संसद के तीन अंग है।- राष्ट्रपति (अनुच्छेद-52) - भारत का सर्वोच्च नागरिक — अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव
- राज्य सभा (अनुच्छेद 80) - उच्च सदन — अप्रत्यक्ष रीति से चुनाव
- लोकसभा (अनुच्छेद 81) - निम्न सदन — प्रत्यक्ष रीति से चुनाव (जनता का सदन भी कहा जाता है।
संसद का गठन
1954 में राज्य परिषद के स्थान पर राज्यसभा एवं जनता का सदन को "लोकसभा" नाम दिया गया ।
भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन राष्ट्रपति, संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता , जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति ना दे दे। राष्ट्रपति संसद के कुछ चुनिंदा कार्य भी करता है।
सदनों की संरचना
राज्यसभा की संरचना
राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इनमें में 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि (अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित) होंगे, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इनमें 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चार संघ राज्य क्षेत्रो का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।
संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है।
राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन
1. राज्यों का प्रतिनिधित्व : राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।2. केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व : राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रत्येक प्रतिनिधि इस कार्य के लिए निर्मित एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
3. मनोनीत सदस्य : राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। (12 सदस्यों के मनोनीत की नीति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है)
राज्य सभा सदस्य बनने की योग्यता
- भारत का नागरिक हो
- 30 वर्ष की आयु हो
- लाभ के पद पर ना हो
राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
- अप्रत्यक्ष रीति (विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा )
राज्य सभा सदस्यों का कार्यकाल
- 6 वर्ष
- एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं
- कभी विघटन नहीं होता है।
- राज्य सभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है।
लोकसभा की संरचना
लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं। एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करता है।वर्तमान समय में लोकसभा में 545 सदस्य है इनमें से 530 से 10 राज्यों, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित या नाम एंग्लो निर्देशित इंडियन समुदाय से हैं।
- राज्यों का प्रतिनिधित्व - राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है उसे मतदान करने का अधिकार है। सन् 1988 में 61 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
- केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व - संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं।
- मनोनीत सदस्य - अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो तो राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत कर सकते हैं
लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता
- भारत का नागरिक हो
- 25 वर्ष की आयु हो
- लाभ के पद पर ना हो
लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन
- प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
- लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन (अनुच्छेद -331)
लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल
- 5 वर्ष (5 वर्ष पश्चात स्वत: भंग)
- मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद में प्रस्ताव पारित कर (एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है)
लोकसभा अध्यक्ष का चयन कुल लोकसभा सदस्य में ही किसी एक को चुना जाता है
लोकसभा के कार्य
- विधेयकों को पारित करना
- धन विधेयक पर एकाधिकार
- मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना
लोकसभा गणपूर्ति या कोरम के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होती है। (सदन में किसी बैठक शुरू करने के लिए निश्चित सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। लोकसभा में 55 और राज्य सभा में 25 )
प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन को दो भागों में बांटा गया है-
(अ) राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन
(ब) प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन।
परिसीमन आयोग
संविधान में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों को लोकसभा क्षेत्रों का आवंटन व प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन के लिए नियमों निर्धारण करें। इसके तहत संसद ने 1952, 1962, 1972 व 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किए।
42वें संशोधन अधिनियम 1976 में राज्यों को लोकसभा क्षेत्रों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। इस प्रतिबंध को 84वें संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों (यानी वर्ष 2026) तक के लिए बढ़ा दिया गया।
लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है - 7.5 लाख
सबसे कम लोकसभा सीट वाले राज्य - सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम
2 लोकसभा सीट वाले राज्य - गोवा, , मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा,
सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य - उत्तर प्रदेश (80) , महाराष्ट्र (48), बिहार (40), मध्यप्रदेश (29) सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति - मध्य प्रदेश
लोकसभा की चुनाव प्रणाली
भारत में लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत पूरे देश को विभिन्न प्रदेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक संसद सदस्य निर्वाचित होते हैं यानी कि प्रत्येक संसद सदस्य एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है
MP और क्षेत्र का अनुपात बराबर होता है जिन राज्यों की संख्या कम है (60 लाख से कम) तो उनके लिए अलग प्रावधान किया गया है।
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में तथा साध्य एक ही हो।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है।
- प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर है।
- महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी है।
संसद सत्र क्या है ?
विधेयक तथा उनके प्रकार
- सरकारी विधेयक
- गैर सरकारी विधेयक
(1) सरकारी विधेयक
(2) गैर सरकारी सदस्यों का विधेयक
- साधारण विधेयक
- धन विधेयक
- वित्त विधेयक
- संविधान संशोधन विधेयक
(1) साधारण विधेयक
संयुक्त बैठक - (अनुच्छेद 108)
(2) धन विधेयक (अनुच्छेद 110)
(3) वित्त विधेयक (अनुच्छेद - 117)
(4) संविधान संशोधन विधेयक
वार्षिक वित्तीय विवरण (अनुच्छेद 112)
बजट
भारत सरकार के दो तरह के बजट होते हैं।
- आम बजट
- रेलवे बजट
भारित व्यय
- राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते तथा उनके कार्यकाल व्यय
- उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा के उपसभापति लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते SC HC न्यायाधीशों के वेतन + भत्ते + पेंशन
- CAG, UPSC, HC+SC+CAG+UPSC — कार्यकाल व्यय
- ब्याज निक्षेप आदि.....
विनियोग विधेयक (अनुच्छेद 114)
- स्थायी व्यय - सरकारी कर्मचारियों की वेतन पेंशन आदि
- अस्थायी व्यय - जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में बहस, मतदान, चर्चा के पश्चात बजट के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।
निधियां
- भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266)
- भारत की लोक लेखा निधि (अनुच्छेद 266)
- भारत की आकस्मिक निधि (अनुच्छेद 267)
भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266 )
संचित निधि - (अनुच्छेद 266)
भारत की लोक निधि (अनुच्छेद 266)
भारत की आकस्मिक निधि या आपातकालीन निधि - (अनुच्छेद 267)
बजट से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली
- लेखानुदान (अंतरिम बजट) - जब संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए बजट ना बनाकर किसी कारणवश कुछ महीनों के लिए ही बजट बनाया जाता है। तो उसे लेखानुदान या अंतिरम बजट कहते हैं।
- प्रत्यानुदान - कुछ ऐसी सेवाएं होती है जिन पर वर्ष के दौरान व्याख्या जाना निश्चित होता है परंतु कितना व्यय होगा। यह निश्चित नहीं होता है इसलिए इसे बजट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। समय आने पर इसके लिए अलग से धन की मांग की जाती है जैसे - 2 अक्टूबर को एक करोड़ पेड़ लगाया जाना है।
- अपवादानुदान - बजट के अतिरिक्त अन्य धन की मांग करना ही अपवादानुदान कहलाता है।
संविधान में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियों
संसद में वाद विवाद (प्रश्नों का स्वरूप)
- तारांकित प्रश्न - ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है तथा जिस पर पूरक प्रश्न (cross questions) पूछ सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों पर बहस होने की संभावना बनी रहती है।
- अतारांकित प्रश्न - ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है तथा जिस पर पूरक प्रश्न (cross questions) नहीं पूछ सकते हैं।
- अल्प सूचना प्रश्न - यदि किसी सदस्य द्वारा पहले से ही पूछे गए जाने वाले प्रश्नों की सूची और मुद्दे सदन को नहीं सौपें गए हैं और तत्कालिक कोई प्रश्न पूछता है तो इसके लिए अध्यक्ष या सभापति को सूचना देकर उनकी स्वीकृति मिलने के पश्चात अल्प सूचना प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

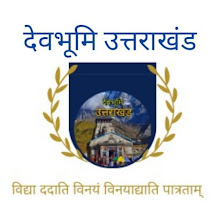

अकल्पनीय अकथनीय अकाट्य अद्वितीय अविस्मरणीय अद्भुत
जवाब देंहटाएं