उत्तराखंड समूह ग मॉडल पेपर Uksssc Mock Test - 231 (1) 'स्मृति की रेखाएं' और 'अतीत के चलचित्र' किसकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएँ हैं? A. सुमित्रानंदन नंदन पंत B. गजानन मुक्तबोध C. महादेवी वर्मा D. मन्नू भण्डारी (2) प्रारूपण है - a) अंतिम दस्तावेज़ जारी करना और प्रिंट के लिए भेजना b) विचारों को व्यवस्थित रूप देना और संरचना प्रदान करना c) मीडिया को सूचना देना और जनता तक पहुंचाना d) गोपनीय पत्र लिखना (3) निम्न को सुमेलित कीजिए (a) बिजली (1) सुरभि (b) यमुना (2) तरुणी (c) गाय (3) अर्कजा (d) स्त्री (4) वितुंडा कूट : (a) (b) (c) (d) (A) 3 2 4 1 (B) 2 3...
हिन्दी वर्णमाला (देवनागरी लिपि)
हिंदी शब्द फारसी ईरानी भाषा का शब्द है। भाषा - भाष् (संस्कृत) की धातु से उत्पन्न होकर बनी है, जिसका का अर्थ है. 'प्रकट करना' । हिंदी सहित सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है.
भाषा का विकास
1. वैदिक संस्कृत (1500 ई.पू. से 1000 ई. पू.)
2. लौकिक संस्कृत (1000 ई.पू. से 500 ई. पू.)
3. पाली (500 ई.पू. से 1 ई.पू. - बौद्ध ग्रंथ )
4. प्राकृत (1 ई.पू. से 500 ई. - जैन ग्रंथ)
5. अपभ्रंश (शोरसैनी) (500 ई से 1000 ई.)
6. हिंदी (1000 ई. से वर्तमान समय में)
*1100 ई. को हिंदी भाषा का मानक समय माना जाता है
वर्णमाला
वर्ण क्या है?
उच्चारित ध्वनियों को जब लिखकर बताना होता है तब उनके लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाएं जाते हैं ध्वनियों को व्यक्त करने वाले ये लिपि - चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। हिन्दी में इन वर्णों को 'अक्षर' कहा जाता है।
वर्णमाला
वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में पहले 'स्वर वर्णों तथा बाद में व्यंजन वर्णों' की व्यवस्था है।
हिंदी लिपि के चिन्ह
अ आ इ ई उ ऊ ऋ
ए ऐ ओ औ अं अः
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व श
ष स ह
क्ष त्र ज्ञ
*महत्वपूर्ण तथ्य
- देवनागरी लिपि का अंतिम चिन्ह ज्ञ
- हिंदी वर्णमाला का अंतिम चिन्ह ह
- अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई - शब्द
- भाषा की सबसे छोटी इकाई - वर्ण
- भाषा की सार्थक इकाई - वाक्य
वाक्य - उपवाक्य - पदबंध - पद (शब्द) - अक्षर - ध्वनि या वर्ण
जैसे राम एक शब्द हैं, जिसमें
2 अक्षर हैं रा और म ।
4 वर्ण हैं - र्, आ, म, अ
प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। यह वर्ण एक निश्चित समूह में होते हैं। वर्णों के ऐसे समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 44 (11 स्वर + 33 व्यंजन) है। किन्तु लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या 52 है । जिसमें शामिल हैं - 44 + 2 आयोगवाह + 2 आगत व्यंजन + 4 संयुक्त व्यंजन
वर्णों के भेद
उच्चारण एवं प्रयोग के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं।
1. स्वर
2. व्यंजन
[1] स्वर किसे कहते हैं
जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है -
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ
स्वरों के तीन भेद होते हैं -
(1) उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर
- ह्रस्व / लघु / मूल / एकमात्रिक स्वर
- दीर्घ स्वर ( सजातीय और विजातीय)
- प्लुप्त स्वर
- ह्रस्व स्वर - जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्योंकि इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनकी संख्या चार (4) है - अ, इ, उ, ऋ। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर या लघु स्वर भी कहा जाता है।
- दीर्घ स्वर - जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं इनकी संख्या सात (7) है - आ, ई, ऊ, ऐ, ऐ ओ, औ।
- प्लुप्त स्वर - जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है, उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है। इनका प्रयोग प्राय: पुकारते समय किया जाता है; जैसे ओऽम्, राऽम् आदि।
(2) ओष्ठ आकृति के आधार पर
- वृताकार स्वर - जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के आकार के हो जाते हैं वृताकार स्वर कहलाते हैं। जैसे - उ, ऊ, ओ, औ
- अवृताकार स्वर - जिनके उच्चारण में होंठ वृत्त के आकार के नहीं होते हैं। अवृताकार स्वर कहलाते हैं । जैसे - अ, आ, इ, ई, ॠ, ए, ऐ
(3) जिव्हा की क्रियाशीलता के आधार पर
- अग्र स्वर - जिनके उच्चारण में जिव्हा का आगे का भाग क्रियाशील रहता है अग्र स्वर कहलाते हैं जैसे - इ, ई, ए, ऐ, ॠ
- मध्य स्वर - वे स्वर जिनके उच्चारण में जिव्हा समान अवस्था में रहती है। मध्य स्वर कहलाते हैं जैसे - अ
- पश्च स्वर - जिनके उच्चारण में जिव्हा का पिछला भाग क्रियाशील रहता है। पश्च स्वर कहलाते हैं। जैसे - उ, ऊ, ओ, औ
(4) मुखाकृति के आधार पर
- संवृत स्वर - इस प्रकार के स्वरो में मुख वृत्त के समान बंद सा रहता है अर्थात मुख सबसे कम खुलता है जैसे - इ, ई, उ, ऊ, ॠ
- विवृत स्वर - इस प्रकार के स्वर में मुख सबसे अधिक खुलता है अर्थात वृत्त के समान खुलता है। जैसे - आ
- अर्धविवृत्त स्वर - इस प्रकार के स्वर में मुख्य विवृत के समान लगभग आधा खुलता है जैसे अ, ऐ, ओ
- अर्ध संवृत स्वर - जिनके उच्चारण में मुख संवृत स्वरों की तुलना में आधा बंद रहता है अर्थ सवृत स्वर कहलाते हैं। जैसे - ए, ओ
(5) नासिका के आधार पर
- निरनुनासिक - जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग नहीं किया जाता है अर्थात सिर्फ मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनिया निरनुनासिक है । जैसे - सभी स्वर
- अनुनासिक स्वर - इस प्रकार के स्वर में उच्चारण मुख्य नाक दोनों से होता है जैसे - अँ आँ इँ ईं उँ ऊँ एँ ऐं ओं औं
- अनुस्वार - इसका उच्चारण नाक से होता है तथा इसका चिन्ह (ं) वर्णो के ऊपर लगता है, जैसे - हंस, पतंग, गंध, गंगा, संसार, आरंभ, प्रियंका आदि।
- अनुनासिक - इसका उच्चारण मुंँह और नाक दोनों से होता है तथा इसका चिन्ह (ँ) भी वर्णों के ऊपर लगता है; जैसे - आँख, गाँव, अँगूठा, पाँच, दाँत आदि।
- विसर्ग - इसका उच्चारण 'ह्' के समान होता है तथा इसका चिन्ह ( : ) वर्णों के आगे लगता है; जैसे- प्रात:, दु:ख, अत:, छ:, आदि।
[2] व्यंजन किसे कहते हैं?
जिन वर्णों के उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या तैंतीस (33) है-
क ख ग घ ङ
च छ ज झ ञ
ट ठ ड ढ ण
त थ द ध न
प फ ब भ म
य र ल व
श ष स ह
व्यंजनों के भेद
(क) स्पर्श व्यंजन
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालू, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ का स्पर्श करके मुख से बाहर आती हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या पच्चीस (25) है - क ख ग घ ङ च छ ष ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म
- स्पर्शी व्यंजन :- इनकी संख्या 16 है। जो इस प्रकार हैं - क ख ग घ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ
- स्पर्श संघर्षी व्यंजन :- च वर्ग के चार वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहा जाता है जैसे - च छ ज झ
- पंचम अक्षर/नासिक्य व्यंजन - वे व्यंजन जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग किया जाता है नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं इन्हें पंचम वर्ण भी कहा जाता है जैसे - ङ ञ ण न म
- उत्क्षिप्त व्यंजन - वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिव्हा ऐसा महसूस कराती है जैसे इन्हें फेंक रही हो इन व्यंजनों को ताङनजात द्विगुण द्विपृष्ठ भी कहा जाता है। जैसे - ड़ ढ़
जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है, उन्हें अंत:स्थ व्यंजन कहते हैं।
इनकी संख्या चार (4) है - य, र, ल, व ।
(ग) ऊष्म व्यंजन -
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी चार (4) है - श, ष, स, ह । संघर्ष के कारण वायु गर्म हो जाती है जिस कारण इन व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है।
- प्रकंपित या लुंठित व्यंजन - वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिव्हा दो से तीन बार कंपन करती है उन्हें प्रकम्पित व्यंजन कहा जाता है । जैसे - र
- पाश्विक व्यंजन - जिनके उच्चारण में जिव्हा ह मसूड़े को छुती है और हवा का प्रमुख वेग जिव्हा के आसपास से निकल जाता है पाश्विक व्यंजन कहलाते हैं जैसे - ल
- संघर्षहीन व्यंजन - जिनके उच्चारण में संघर्ष नहीं होता है वह संघर्ष हीन व्यंजन कहलाते हैं इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे - य, व
इन व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और भी व्यंजन हैं किन्तु ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं हैं बल्कि अन्य व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ये दो प्रकार के माने गए हैं -
(1) संयुक्त व्यंजन
(2) द्वित्व व्यंजन
1. संयुक्त व्यंजन - दो भिन्न व्यंजनों के मेल से वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या चार (4) है -
क् + ष = क्ष - क्षति, क्षत्रिय, क्षमा
ज् + ञ = ज्ञ - ज्ञान, ज्ञानी, यज्ञ
त् + र = त्र - पत्र, इत्र, त्रिशूल
श् + र = श्र - श्रवण, श्रम श्रद्धा
2. द्वित्व व्यंजन - दो समान या एक जैसे व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं; जैसे -
क् + क = क्क - शक्कर, चक्की, मक्का
च् + च = च्च - सच्चाई, बच्चा, कच्चा
ग् + ग = ग्ग - बुग्गी, झुग्गी, दिग्गज
म् + म = म्म - चम्मच, सम्मान, निकम्मा
आगत ध्वनियांँ
हिंदी भाषा में कुछ ध्वनियां विदेशी भाषाओं से भी आई हैं। ऐसी ध्वनियों को आगत ध्वनियांँ कहते हैं; जैसे -
आॕ - इस ध्वनि का प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के ठीक उच्चारण के लिए किया जाता है। इसका चिन्ह अर्धचंद्राकार (ॕ) है; जैसे -
डाॅक्टर, प्राॅक्टर, बाॕॅल, हाॅल आदि।
ज़ - इस ध्वनि का प्रयोग उर्दू, फ़ारसी, तुर्की आदि शब्दों में किया जाता है; जैसे - ज़ब्त, ज़मीन, मज़हब, ज़बानी आदि।
फ़ - इस ध्वनि का प्रयोग भी उर्दू, फ़ारसी, तुर्की आदि शब्दों में किया जाता है; जैसे - फ़न, फ़तह, फ़ना, फ़रिश्ता आदि ।
विकसित व्यंजन - 'ङ' तथा 'ढ़' वर्ण 'ड' तथा 'ढ' के विकसित रूप हैं, इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है, जैसे - बड़ा, सड़क, गढ़, चढ़ाई आदि।
'र' का संयोग
हिंदी वर्णमाला में 'र' एक ऐसा वर्ण है जिसका अन्य व्यंजनों के साथ संयोग होने पर उसका रूप भिन्न हो जाता है। 'र' के संयोग के कुछ नियम निम्नलिखित हैं -
1. यदि 'र्' ( स्वर रहित) के बाद कोई व्यंजन आता है, तो यह उस व्यंजन के ऊपर रेफ (॑) के रूप में लगता है; जैसे -
र् + म = र्म (धर्म, शर्म)
र् + द = र्द (मर्द, दर्द)
र् + च = र्च (चर्च, खर्च)
र् + व = व (पूर्व, गर्व )
2. यदि 'र' से पहले कोई 'अ' रहित व्यंजन आता है, तो यह उसके साथ पदेन (,) के रुप में लगता है; जैसे -
क् + र = क्र (क्रम, क्रय)
प् + र = प्र (प्रयास, प्रतिज्ञा)
म् + र = म् (नम्र, आम्र)
ग् + र = ग्र ( ग्रह, ग्रहण )
3. जब 'र' से पहले स्वर रहित 'ट्' या 'ड्' आता है, तो यह उनके नीचे पदेन (^) के रूप में लगता है; जैसे -
ट् + र = ट्र (ट्रक, ट्रेन)
ड् + र = ड्र ( ड्रम, ड्रामा)
वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं
किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग-अलग करके लिखने की प्रक्रिया वर्ण- विच्छेद कहलाती है; जैसे -
रोहन = र् + ओ + ह् + अ + न् + अ
नवनीत = न् + अ + व् + अ + न् + ई + त + अ
परिश्रम = प् + अ + र् + इ + श् + र् + अ + म् + अ
शब्द - विचार
हमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है;जैसे -
त् + ओ + त् + आ = तोता
ग् + उ + ल् + आ + ब् + अ = गुलाब
म् + अ + छ् + अ + ल् + ई = मछली
स्वरतंत्रयों कंपन के आधार पर वर्ण
- अघोष वर्ण - जिन वर्णों में गूंज या कंपन नहीं होता है वह वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं । प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क ख च छ ट ठ त थ प फ श ष स (13)
- सघोष वर्ण - जिनके उच्चारण में गूंज या कंपन होता है सघोष वर्ण कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण ( ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ण द ध न ब भ म य र ल व ह और सभी स्वर )
प्राण वायु और श्वास के आधार पर
- अल्पप्राण – जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। अल्पप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण को अल्पप्राण कहा जाता है ( क ग ङ च ज ञ ट ड ण त द न प ब म य र ल व और सभी स्वर )
- महाप्राण - जिनके उच्चारण में मुख्य विवर से ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है महाप्राण वर्ण कहलाते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण (ख घ छ झ ठ ढ थ ध फ भ) इसके अलावा श ष स ह को भी महाप्राण कहा जाता है।
उच्चारण स्थान के आधार पर
1. कंठ्य वर्ग - अकुहविसर्जियांकंठ (अ आ क वर्ग ओर ह)
2. तालुवर्ग - इचुयशानांतालु (इ ई च वर्ग य ओर श)
3. मूर्धा - ऋटूरषाणांममूर्धा (ऋ ट वर्ग र और ष)
4. दन्त - तुलसानीदन्तस्य (त वर्ग ल और स)
5. ओष्ठ - उपूपध्यमानीयानांओष्ठ (उ ऊ प वर्ग)
6. नासिक्य - (ङ ञ ण न म)
7. वत्स्र्य (मसूड़ा) - (र न ल स ज)
8. एदैतोकंठतालु - (कंठ + तालु : ए ऐ)
9. ओदोतौकंठोष्ठ - (कंठ + ओष्ठ ओ औ)
10. वकारस्य दन्तोष्ठ - (व दन्त + ओष्ठ)
11. काकल्य / अलिजिह्वा - (ह)

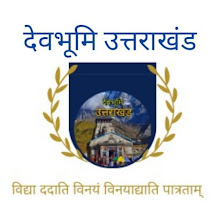

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts.
Please let me now.