उत्तराखंड समूह ग मॉडल पेपर Uksssc Mock Test - 231 (1) 'स्मृति की रेखाएं' और 'अतीत के चलचित्र' किसकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएँ हैं? A. सुमित्रानंदन नंदन पंत B. गजानन मुक्तबोध C. महादेवी वर्मा D. मन्नू भण्डारी (2) प्रारूपण है - a) अंतिम दस्तावेज़ जारी करना और प्रिंट के लिए भेजना b) विचारों को व्यवस्थित रूप देना और संरचना प्रदान करना c) मीडिया को सूचना देना और जनता तक पहुंचाना d) गोपनीय पत्र लिखना (3) निम्न को सुमेलित कीजिए (a) बिजली (1) सुरभि (b) यमुना (2) तरुणी (c) गाय (3) अर्कजा (d) स्त्री (4) वितुंडा कूट : (a) (b) (c) (d) (A) 3 2 4 1 (B) 2 3...
राजी जनजाति का संपूर्ण परिचय
उत्तराखंड की जनजातियां (भाग - 5)
राजी जनजाति उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में निवास करने वाली एक अत्यंत छोटी और लुप्तप्राय अनुसूचित जनजाति है। इसे "बनरौत" या "जंगल का राजा" के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लोग मुख्यतः जंगलों में रहते हैं और प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव रखते हैं। राजी जनजाति की आबादी बहुत कम है, और यह विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसकी स्थिति पर चिंता जताई है।
राजी जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन और आदिम जनजातियों में से एक है। यह माना जाता है कि ये लोग प्राचीन काल से पिथौरागढ़ और चंपावत के जंगलों में निवास करते आए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि राजी जनजाति का संबंध प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड या ऑस्ट्रो-एशियाटिक समूहों से हो सकता है, जो प्राचीन भारत में बसे थे। उनकी बोली, जिसे "मुण्डा" कहा जाता है, में तिब्बती और संस्कृत शब्दों की अधिकता देखी जाती है, जो उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों को दर्शाती है। राजी जनजाति के लोग काष्ठ कला में निपुण होते हैं और उनके आवासों को रौत्यूड़ा कहा जाता है।
2001 की जनगणना के अनुसार, राजी जनजाति की जनसंख्या लगभग 528 थी, जो 2011 तक बढ़कर लगभग 800-900 तक पहुंची। यह जनजाति मुख्यतः पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट, और कनालीछीना विकासखंडों के 10 गांवों में, चंपावत के एक गांव में और कुछ संख्या में ऊधम सिंह नगर में निवास करती है। जबकि यह जनजाति मुख्य रूप से पिथौरागढ़ के धारचूला, डीडीहाट विकासखंड के 7 गांव में निवास करती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, वे स्वयं को राजपूत वंश से जोड़ते हैं, जो संभवतः उनकी सामाजिक पहचान को मजबूत करने का प्रयास है।
अफ्रीकी नीग्रो, आस्टिक और मंगोलॉयड प्रजातियाँ विश्व भर में फैलीं तथा अपने प्रसार के साथ भिन्न-भिन्न भागों में बस गयीं।
इनमें मंगोलॉयड वर्ग के लोगों ने उच्च हिमालय में अपने को अवस्थित किया और अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुए।
ऐतिहासिक अवलोकन
आर्यों के आगमन से पूर्व इस हिमाालय क्षेत्र में यक्ष, किन्नर, किरात, नाग, मल्ल, खस, आदि अपना प्रभुत्तव जमा चुके थे। इन प्रजातियों में क्या संबंध थे ? यह कहना कठिन हैं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं उनमें जातीय समानता, निकटता या सम्मिश्रण की स्थिति सक्रिय रही होगी। एक समय समस्त पर्वतीय क्षेत्र में आस्टिक और आदि मंगोलॉयड लोग फैले थे। भारतीय साहित्य में मंगोलॉयड लोगों के लिए किरात् शब्द का प्रयोग हुआ है। इन्हें गढ़वाल कुमाऊँ और नेपाल में किराती राजी आदि नामों से पुकारा जाता है। किरातों का उल्लेख अथर्ववेद में आया है। महाभारत में हिमवदुर्ग निलया, किरात, कहा गया हैं। हिमालय के पश्चिमी भाग में किन्नर थे तो पूर्व में किरात। एक समय कोसी के पूर्व में बसने वाली राई, लिम्बू, याख्या आदि जातियाँ किरात ही कही जाती थीं जिन्हें राजी कहा जाता है।
वस्तुतः चपटी मुखाकृति पीला गेहुआँ रंग के लोग लद्दाख से लेकर असम तक फैले हैं। लद्दाख के मोटा स्थिति के सिपत्माल, मलाण गाँव की मलाणी, नेलड़ के जाड़, नीति के मार्छा-तोर्छा, मिलम के जौहारी शौका, अस्कोट के राजी, नेपाल के माख्या राई, लिम्बू तथा असम के लेप्चा आदि उस प्राचीन प्रजाति से संबंधित हैं जिसे मोनख्योर पुकारा जाता है।
डॉ. शिव प्रसाद डबराल यह मानते हैं कि पश्चिम से खष्, दरद् जाति के प्रसार के साथ आगे चलकर कई मिश्र जातियों की प्रभुता के कारण किरातों का अस्तित्व खतरे में पड गया। आर्यों ने उन्हें प्रबल प्रतिद्वन्दी के रूप में लिया। किरातों के साथ मुण्डों का वर्णन प्राचीन साहित्य के अनेक स्थलों पर मिलता है। यह जाति पराजित हुई और अपने को सिकोड़ - सिमट कर रखने को बाध्य हुई। यही कारण है कि किरातों का रक्त औरों में मिश्रित हुआ। किंतु किरात जाति उत्तरी सीमा में ही अपने को बचा पाई। इन्हीं की विभिन्न शाखाएँ विभिन्न नामों से भिन्न-भिन्न स्थानों पर रह रही हैं। डॉ. राहुल सांकृत्यायन मानते हैं कि इनका संबंध चीनी-तिब्बती मंगोलीय जाति से था।
राजी जनजाति का संबंध शक् जातियों से भी जोड़ा जा सकता हैं। शक् पशुचारक और घुमंतू थे। राहुल सांकृत्यायन के शब्दों में यह मानने के लिए पर्याप्त प्रमाण मिलेंगे कि भव्य हिमालय के शकों का शासन नहीं बल्कि यहां का प्रतापी कत्यूरी भी उन्हीं में से संबंधित था। शक कई प्रकार के थे और वे मूलतः शकस्थान और सीरकांठा में निवास करते थे, 170 ई.पू. मे शक अपने मूल स्थान पूर्वी सिड़क्यांग को छोड़कर पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान होते हुए भारत में आए।
राजी जनजाति का मुख्य निवास : पिथौरागढ़
सन् 1960 से पूर्व पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जनपद की एक तहसील थी। 24 फरवरी 1960 को, पिथौरागढ़ को जनपद के रूप में मान्यता मिली। तात्कालिक समय में पिथौरागढ़ को चार तहसीलों (पिथौरागढ़, धारचूला, डीडीहाट, मुनस्यारी) में विभक्त किया गया। वर्तमान में इस जनपद में कुल आठ तहसील विण, मूनाकोट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, धारचूला, मुनस्यारी, डीडीहाट एवं कनालीछीना हैं। जनपद की उत्तरी सीमा पर स्थित (धारचूला, कनालीछीना, डीडीहाट) तहसील में राजी जनजाति निवास करती है।
सामाजिक स्थिति
राजी जनजाति की सामाजिक संरचना सरल और परंपरागत है। ये लोग सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव में रहते हैं और बाहरी दुनिया के साथ संपर्क में संकोच करते हैं, जो उनकी सामाजिक स्थिति को और कमजोर करता है। उनकी सामाजिक व्यवस्था परिवार-केंद्रित है, और कई परिवार मिलकर छोटे गांव बनाते हैं। उनके आवास, जिन्हें "रौत्यूड़ा" कहा जाता है, ज्यादातर जंगलों में बने होते हैं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होते हैं।
राजी जनजाति में पहले पलायन विवाह का प्रचलन था। राजी जनजाति में विवाह दो परिवारो के बीच समझौता माना जाता है। विवाह से पूर्व राजी जनजाति में सांगजांगी, पिंठा संस्कार प्रथा प्रचलित है। राजियों में वधू-मूल्य प्रथा का प्रचलन है। राजी जनजाति में विवाह-विच्छेद के लिए स्त्रियों-पुरूषों को समान अधिकार प्राप्त हैं स्त्रियों को परदे में रखने व रसोई में किसी दूसरे व्यक्ति को प्रवेश न देने की परम्परा है
संस्कृति और परंपराएं : राजी जनजाति की संस्कृति प्रकृति-केंद्रित है। वे रिंग डांस (थड़िया नृत्य के समान) करते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। उनकी बोली "मुण्डा" में तिब्बती और संस्कृत शब्दों का प्रभाव है, और यह उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को दर्शाती है।
धार्मिक व्यवस्था - राजी जनजाति के प्रमुख त्योहार कर्क व मकर संक्राति है। वे हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों का पालन करते हैं, लेकिन उनकी पूजा में स्थानीय देवी-देवताओं और प्रकृति की पूजा का समावेश होता है। राजी जनजाति के प्रमुख देवता बाघनाथ है, यह लोग गणनाथ, मलैनाथ, मल्लिकार्जुन व घुरमल देवी-देवता की पूजा करते है
भाषा : राजी कुमाऊँनी का प्रयोग करते हैं किन्तु उनकी अपनी बोली भी है। इस जनजाति से तिब्बती संस्कार विलुप्त हो चुके हैं। भाषा तिब्बती प्रभाव को आँक सकती है किन्तु जाति के स्वरूप को निर्धारित नहीं कर सकती है।
शिक्षा और स्वास्थ्य : राजी जनजाति में शिक्षा का स्तर बहुत कम है, जिसके कारण वे सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुविधाओं से वंचित रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और जागरूकता का अभाव उनकी सामाजिक स्थिति को और कमजोर करता है।
आर्थिक स्थिति,
राजी जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है, और वे अभी भी आदिम परिस्थितियों में जीवनयापन करते हैं। उनकी आजीविका मुख्यतः जंगल के संसाधनों पर आधारित रही है, लेकिन अब वे धीरे-धीरे कृषि और दस्तकारी की ओर बढ़ रहे हैं। यह जनजाति झूम विधि से खेती करती है, और ये लोग अदृश्य विनिमय प्रणाली का प्रयोग करते हैं।
पारंपरिक आजीविका : पहले राजी जनजाति जंगली लकड़ी, शहद, फल-फूल, कंदमूल, और जंगली जानवरों के शिकार पर निर्भर थी। अब उनकी अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, और छोटे स्तर की दस्तकारी (जैसे डलिया, बर्तन, और जाल बनाना) पर आधारित है।
ग्रामीण योजना और कार्रवाई संघ (अर्पण) जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने राजी जनजाति की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सुझाव दिए हैं, जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना। इसके अलावा, सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इनका लाभ राजी जनजाति तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है।
राजनीतिक स्थिति
राजी जनजाति की राजनीतिक स्थिति भी उनकी छोटी जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण कमजोर है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व : संविधान के अनुच्छेद 243D के तहत पंचायत राज संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है, जिससे राजी जनजाति को स्थानीय स्तर पर कुछ राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है। हालांकि, उनकी छोटी जनसंख्या के कारण उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित है। राजी जनजाति से संबंधित प्रथम विधायक गगन सिंह रजवार हैं, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी का एक उदाहरण हैं।
सरकारी नीतियां और संरक्षण : संविधान का अनुच्छेद 46 अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने और सामाजिक शोषण से उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य को देता है। इसके तहत, केंद्र और राज्य सरकारों ने जनजातीय कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं, जैसे अनुदान, अनाज बैंक, और शिक्षा के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति। हालांकि, इन योजनाओं का कार्यान्वयन राजी जनजाति के लिए अपर्याप्त रहा है।
निष्कर्ष
राजी जनजाति उत्तराखंड की एक अनूठी और लुप्तप्राय जनजाति है, जो अपनी विशिष्ट संस्कृति और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव के लिए जानी जाती है। हालांकि, उनकी सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। सामाजिक अलगाव, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, आर्थिक पिछड़ापन, और सीमित राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनकी प्रमुख चुनौतियां हैं। उत्तराखंड सरकार और गैर-सरकारी संगठनों ने उनकी स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन इनका प्रभाव सीमित रहा है। राजी जनजाति के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए कृषि भूमि, रोजगार, शिक्षा, और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि यह जनजाति विलुप्त होने से बच सके और मुख्यधारा में शामिल हो सके।
स्रोत : पिथौरागढ़ के राजी समुदाय की समाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति (जितेन्द्र बहादुर मिश्र)
Related post :

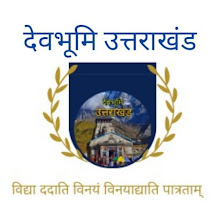
.jpg)
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts.
Please let me now.