उत्तराखंड समूह ग मॉडल पेपर Uksssc Mock Test - 231 (1) 'स्मृति की रेखाएं' और 'अतीत के चलचित्र' किसकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएँ हैं? A. सुमित्रानंदन नंदन पंत B. गजानन मुक्तबोध C. महादेवी वर्मा D. मन्नू भण्डारी (2) प्रारूपण है - a) अंतिम दस्तावेज़ जारी करना और प्रिंट के लिए भेजना b) विचारों को व्यवस्थित रूप देना और संरचना प्रदान करना c) मीडिया को सूचना देना और जनता तक पहुंचाना d) गोपनीय पत्र लिखना (3) निम्न को सुमेलित कीजिए (a) बिजली (1) सुरभि (b) यमुना (2) तरुणी (c) गाय (3) अर्कजा (d) स्त्री (4) वितुंडा कूट : (a) (b) (c) (d) (A) 3 2 4 1 (B) 2 3...
कोठारी आयोग : शिक्षा का एक ऐतिहासिक दस्तावेज
1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) से पूर्व, भारत की शिक्षा व्यवस्था औपनिवेशिक प्रभावों और व्यापक असमानताओं से ग्रस्त थी। 1854 की "वुड्स शिक्षा प्रणाली" ने औपनिवेशिक शिक्षा का आधार तैयार किया, जिसमें अंग्रेजी भाषा, पश्चिमी ज्ञान और रटने पर अत्यधिक ज़ोर दिया गया। उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी गई, जबकि प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित रही। शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश शासन में सहायक बनाना था।
इस प्रणाली ने विभिन्न प्रकार के विद्यालयों (सरकारी, मिशनरी, निजी) में शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता में भारी असमानताएं पैदा कीं। जाति, लिंग और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव व्याप्त था। लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा तक पहुंच अत्यंत सीमित थी। उस समय पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक ज्ञान और रटने पर ज़ोर दिया गया था, जबकि व्यावहारिक शिक्षा और कौशल विकास को नजरअंदाज किया गया था। शिक्षा का मूल्यांकन मुख्य रूप से परीक्षाओं पर आधारित था, जिसके कारण रटने और परीक्षा में सफल होने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया गया।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षा
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारत सरकार ने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का आधार स्तंभ माना और शिक्षा व्यवस्था में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। इन परिवर्तनों का उद्देश्य शिक्षा को अधिक सुलभ, न्यायसंगत और प्रासंगिक बनाना था।
स्वतंत्रता के पश्चात 1948 भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए डॉ. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में "विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग" का गठन किया गया। इस आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे "राधाकृष्णन आयोग रिपोर्ट" के नाम से जाना गया। तथा माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु 23 सितंबर 1952 को शिक्षाविद् डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' की स्थापना की। जिसे मुदालियर आयोग भी कहा गया।
कोठारी आयोग की स्थापना
भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 को शिक्षा प्रणाली का आकलन करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने के लिए "डॉ. दौलत सिंह कोठारी" की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इसे 'कोठारी आयोग' के नाम से जाना जाता है।
मुख्य उद्देश्य :
इस आयोग का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना और सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए राष्ट्रीय नीति और सिद्धांतों की सिफारिश करना था। यह रिपोर्ट शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और आज भी भारतीय शिक्षा नीति पर चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाना।
- शिक्षा को जीवन, आवश्यकताओं और लोगों की आकांक्षाओं से जोड़ना।
- सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण बनाना।
आयोग के सुझाव व सिफारिशें
'आयोग' ने शिक्षा के सभी अंगों के विषय में अपने विचार व्यक्त किये अंग निम्नलिखित है- है। इनमें से महत्त्वपूर्ण
1. शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य
- शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना
- शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करना।
- शिक्षा द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाना
- शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तीव्रता लाना।
- शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र का निर्माण करना
2. शिक्षा की संरचना एवं स्तर
3. अध्यापक की स्थिति
4. अध्यापक शिक्षा
5. छात्र संख्या एवं जनबल
6. शैक्षिक अवसरों की समानता
7. विद्यालय शिक्षा का विस्तार
8. विद्यालय पाठ्यक्रम
9. शिक्षण-विधियों, निर्देशन एवं मूल्यांकन
10. उच्च शिक्षा
11. स्त्री शिक्षा
12. वयस्क शिक्षा
13. विज्ञान की शिक्षा
14. कृषि की शिक्षा
15. व्यावसायिक, प्राविधिक एवं इंजीनियरिंग की शिक्षा
शिक्षा की संरचना व स्तर
आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना अर्थात् ढाँचे और शिक्षा स्तरों के उन्नयन के सम्बन्ध में विचार अभिव्यक्त किये हैं, हम उनका वर्णन निम्नांकित शीर्षकों के अन्तर्गत कर रहे सम्बन्ध
(1) विद्यालय शिक्षा की नवीन संरचना - 'आयोग' ने सामान्य शिक्षा के प्रचलित स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, इस शिक्षा की नवीन संरचना को इस प्रस्तुत किया है-
- 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा
- 2 या 3 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा
- 2 या 3 वर्ष की निम्न माध्यमिक शिक्षा
- 3 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा
- 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक शिक्षा
- 1 से 3 वर्ष की पूर्व-विद्यालय शिक्षा
कोठारी आयोग की शिक्षा प्रणाली का 10+2+3 पैटर्न पर आधारित थी। जिसमें प्राथमिक शिक्षा (1-5), माध्यमिक शिक्षा (6-8), उच्च माध्यमिक शिक्षा (9-10), स्नातक शिक्षा (3 वर्ष)
और स्नातकोत्तर शिक्षा (2 वर्ष) थी
और स्नातकोत्तर शिक्षा (2 वर्ष) थी
कोठारी आयोग का प्रभाव
- कार्यात्मक शिक्षा : कोठारी आयोग ने शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सिफारिश की कि स्कूली शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को शामिल किया जाए। ताकि छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप, भारत में कई व्यावसायिक और तकनीकी स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए।
- व्यावसायिक शिक्षा : कोठारी आयोग ने रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की। उन्होंने सिफारिश की कि सरकार व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए अधिक संसाधन आवंटित करे। इस सिफारिश के परिणामस्वरूप, भारत में कई सरकारी और गैर-सरकारी व्यावसायिक शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए।
- शिक्षा में समानता : कोठारी आयोग ने लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और समान अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा में समानता लाने पर जोर दिया। उन्होंने लड़कियों और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए कई सिफारिशें कीं। इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप, लड़कियों और वंचित वर्गों के शिक्षा में नामांकन दर में वृद्धि हुई।
- शिक्षकों का प्रशिक्षण और कल्याण : कोठारी आयोग ने शिक्षकों के बेहतर प्रशिक्षण और सेवा शर्तों के लिए सिफारिशें कीं। उन्होंने शिक्षकों को अधिक पेशेवर और सम्मानित बनाने के लिए कई उपाय किए। इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत में शिक्षकों के प्रशिक्षण और कल्याण में सुधार हुआ।
- शिक्षा का विकेंद्रीकरण : कोठारी आयोग ने शिक्षा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के लिए शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने की सिफारिश की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई उपाय किए।इन सिफारिशों के परिणामस्वरूप, भारत में शिक्षा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भूमिका बढ़ी।
- शिक्षा का वित्तपोषण : कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए अधिक संसाधन जुटाने की सिफारिश की। उन्होंने शिक्षा पर सरकारी खर्च बढ़ाने और शिक्षा के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई उपाय किए
संविधान के साथ संबंध
शिक्षा का मौलिक अधिकार : भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कोठारी आयोग ने इस अधिकार को लागू करने के लिए कई सिफारिशें कीं, जिनमें शामिल हैं:
- प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए ठोस कदम उठाना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण और कल्याण में सुधार करना।
समानता का अधिकार : संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 शिक्षा में समानता का अधिकार प्रदान करता है। कोठारी आयोग ने सभी नागरिकों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें कीं।
धर्मनिरपेक्षता : संविधान का अनुच्छेद 25 धर्मनिरपेक्षता की गारंटी देता है। कोठारी आयोग ने धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सिफारिशें कीं, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान करते हुए नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना शामिल है।
कोठारी आयोग की सिफारिशों का प्रभाव
कोठारी आयोग की सिफारिशों का भारतीय शिक्षा प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन सिफारिशों ने 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बाद की शिक्षा नीतियों को आकार देने में मदद की।

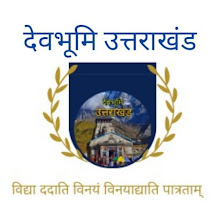
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts.
Please let me now.