उत्तराखंड समूह ग मॉडल पेपर Uksssc Mock Test - 231 (1) 'स्मृति की रेखाएं' और 'अतीत के चलचित्र' किसकी प्रसिद्ध गद्य रचनाएँ हैं? A. सुमित्रानंदन नंदन पंत B. गजानन मुक्तबोध C. महादेवी वर्मा D. मन्नू भण्डारी (2) प्रारूपण है - a) अंतिम दस्तावेज़ जारी करना और प्रिंट के लिए भेजना b) विचारों को व्यवस्थित रूप देना और संरचना प्रदान करना c) मीडिया को सूचना देना और जनता तक पहुंचाना d) गोपनीय पत्र लिखना (3) निम्न को सुमेलित कीजिए (a) बिजली (1) सुरभि (b) यमुना (2) तरुणी (c) गाय (3) अर्कजा (d) स्त्री (4) वितुंडा कूट : (a) (b) (c) (d) (A) 3 2 4 1 (B) 2 3...
उत्तराखंड के लोकगीत और लोक नृत्य
पहाड़ की अपनी ही बोली और संस्कृति है यहाँ के लोक गीतों का विस्तृत स्वरूप मुक्तको के रूप में मिलता है। विभिन्न अवसरों तथा विविध प्रसंगी में मुक्तकों का व्यवहार होता है, पहाड़ी समाज में अपनी विशिष्ट संस्कृति पौराणिक काल से रही है.
न्यौली
इसे न्यौली, न्यौल्या या वनगीत के नामों से पुकारा जाता है, न्यौली का अर्थ किसी नवीन स्त्री को नवीन रुप में सम्बोधन करना और स्वर बदल बदलकर प्रेम परक अनुभूतियों को व्यक्त करना है। न्यौली प्रेम परक संगीत प्रधान गीत है जिसमें दो-दो पंक्ति होती है। पहली पंक्ति प्रायः तुक मिलाने के लिए होती है। न्यौली में जीवन चिन्तन की प्रधानता का भाव होता है।
ब्योली ब्योली रैना, मेरो मन बस्यो परदेश,
कब आलो मेरो सैंया, मेरो मन लियो हदेश।
(अर्थ: रात बीत रही है, मेरा मन परदेश में बसा है। कब आएगा मेरा प्रिय, जिसने मेरा मन ले लिया।)
"सबै फूल फुली यौछ मैथा फुलौ ज्ञान,
भैर जूँला भितर भूला माया भूलै जन,
न्यौली मया भूलै जन",
बैरा (नृत्य गीत)
बैरा का शाब्दिक अर्थ संघर्ष है जो गीत युद्ध के रूप में गायकों के बीच होता है। अर्थात् यह कुमाऊं क्षेत्र का गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में आयोजित होने वाला नृत्य गीत है।
बैरा गाते समय किसी वाध-यंत्र का प्रयोग नही होता है। आज इनका प्रचलन विशेषत: किसी मेले या विशेष उत्सव के शुभ अवसर पर होता है।
"रद्दटै कि तान घट कुला बान,
कैले पाते जातिया जसो, कैका विगध्या दान"
भगनौला गीत
पहाडी गीत संगीत में भगनौना सौन्दर्य विषयक गीत है।
"पाखा की दन्यार सुवा, पाखा की दन्यार,
मूली जौली दाँतपाटी, मै भुलूँ अनार"
ये सौन्दर्य व प्रेम परक उक्तियाँ है जो गाते समय मुख या केन्द्रीय उक्ति से सम्बद्ध कर दी जाती है। मुख्य गायक आलाप लेते हुए आरम्भ में कुछ पंक्तियाँ गाता है फिर हुडका बजाकर अपने साथियों से उसे दुहराने का संकेत करता है।
झोड़ा गीत (नृत्य गीत)
झोड़ा उत्तराखंड का माघ महीने में गाया जाने वाला एक सामूहिक लोकगीत और नृत्य है, जो मुख्य रूप से कुमाऊँ क्षेत्र में प्रचलित है। यह सामाजिक एकता का प्रतीक है और मेले, त्योहारों, और विवाह समारोहों में गाया जाता है। गीतों में प्रेम, प्रकृति, और सामाजिक मूल्यों का वर्णन होता है।
उत्तराखण्ड के गॉंव-गाँव में झोड़ा गायन प्रथा प्रचलित है, इसमें बच्चे, युवा सभी भाग लेते हैं, गाँव के सभी सदस्य वृत्ताकार घेरा बनाते हुए, परस्पर एक दूसरे के कंधों में हाथ रखकर धीमे व सरल पद संचालन के साथ गीत गाना प्रारम्भ करते है। वृत्त के बीच में खड़े होकर मुख्य गायक गीत की प्रथम पंक्ति कहता है, तब अन्य व्यक्ति उसे दोहराते है।
धार्मिक झोड़ों में देवी देवताओं का स्मरण पूजा, विनय आदि की भावना भी प्रकट होती है।
उदाहरण पंक्तियाँ (कुमाऊँनी में):
ओ माया की मायावी, मेरो मन लियो मोहि,
कैं जाणु मैं कुमाऊँ, तेरा रंग रूप देखि।
(अर्थ: हे माया की जादूगरनी, तुमने मेरा मन मोह लिया। मैं कुमाऊँ कैसे जाऊँ, तुम्हारा रूप देखकर।)
विशेषता: ये गीत धीमी और मधुर लय में गाए जाते हैं, और लोग गोलाकार में नृत्य करते हैं।)
चाँचरी (नृत्य गीत)
चांचरी गढ़वाल और कुमाऊँ क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत और नृत्य है। यह प्रेम और रोमांस पर आधारित होता है और अक्सर युवा जोड़ों द्वारा गाया जाता है। इसे झोड़ा की तुलना में अधिक उत्साहपूर्ण और तेज लय में प्रस्तुत किया जाता है।
चाचरी में वृत्ताकार घेरे में गीत गाए जाते है, चाँचरी गीतों में धार्मिक भावना की प्रधानता होती है। स्त्री पुरुष छन्द पर छन्द मिलाकर लम्बे समय तक अविरल गति से नृत्य करते हुए गीत गाते हैं।
उदाहरण पंक्तियाँ:
हाय रे चांचरी, मेरो मन लै ग्यो,
काले काले केशों में, फूलों की माला सज्यो।
(अर्थ: हे चांचरी, तुमने मेरा मन ले लिया, काले-काले बालों में फूलों की माला सजी है।)
चांचरी गीतों में ढोल और नगाड़े की ताल प्रमुख होती है, और यह समूह में गाया जाता है। उत्तराखण्ड के अधिकतर क्षेत्र में मेले, पर्व त्यौहार आदि, अवसरों पर चाँचरी गीत व नृत्य का आयोजन होता है।
छपेली (प्रेम या प्रणय गीत)
छपेली एक नृत्य गीत है, यह गीत दो प्रेमियों का है। दो व्यक्ति, प्रेमी, प्रेमिका, भाई, बहन, पिता, पुत्र कोई भी हो सकते है इसमें भाव सरल व उल्लास पूर्ण होते हैं।
"ओ तिलका तेरी लंबी लूटी के मरि मनै कि हुनी,
के भी मेरी जानी वेराणी जंगणी,
भौजा तेरी नथा नानी".
झुमैलो गीत (प्रणय प्रसंग गीत)
इस गीत में नारी हृदय की वेदना व सौंदर्य का वर्णन मिलता है। यह गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है।
उत्तराखंड के लोकनृत्य
उत्तराखंड के लोकनृत्य अपनी जीवंतता और सामुदायिक भावना के लिए जाने जाते हैं। ये नृत्य अक्सर लोकगीतों के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं और विभिन्न अवसरों पर सामाजिक एकता को दर्शाते हैं। कुछ प्रमुख लोकनृत्य निम्नलिखित हैं:
1. पवाड़ा या भड़ौ नृत्य
पवाड़ा गढ़वाल और कुमाऊँ में वीर रस से भरे गीत हैं, जो ऐतिहासिक योद्धाओं और उनके शौर्य की गाथाएँ सुनाते हैं। ये गीत अक्सर स्थानीय नायकों जैसे तीलू रौतेली या वीर भड़ की कहानियों पर आधारित होते हैं।
उदाहरण पंक्तियाँ:
तीलू रौतेली आली, गढ़वाल की शान,
तलवार उठाय लड़ी, वीरों की पहचान।
(अर्थ: तीलू रौतेली आई, गढ़वाल की शान। तलवार उठाकर लड़ी, वीरों की पहचान।)
2. झोड़ा नृत्य
झोड़ा नृत्य कुमाऊँ क्षेत्र का सामूहिक नृत्य है, जिसमें पुरुष और महिलाएँ गोलाकार में हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। यह धीमी और लयबद्ध गति में किया जाता है। नृत्य के दौरान लोग रंगीन पारंपरिक परिधान पहनते हैं, और ढोल-नगाड़े की ताल पर कदम मिलाते हैं। यह सामाजिक एकता का प्रतीक है।
3. चांचरी नृत्य
चांचरी नृत्य झोड़ा से अधिक तेज और उत्साहपूर्ण होता है। यह प्रेम और उत्सव का प्रतीक है और कुमाऊँ क्षेत्र में लोकप्रिय है।
नर्तक जोड़े में नृत्य करते हैं, और इसमें तेज गति की हरकतें शामिल होती हैं। महिलाएँ घाघरा-चोली और पुरुष कुर्ता-पायजामा पहनते हैं।
4. छोलिया नृत्य (युद्ध नृत्य)
छोलिया कुमाऊँ का एक वीर रस से भरा नृत्य है, जो युद्ध और शौर्य को दर्शाता है। इसे अक्सर विवाह समारोहों में बारात के स्वागत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नर्तक तलवार और ढाल के साथ नृत्य करते हैं, और ढोल-नगाड़े की तेज ताल पर प्रदर्शन करते हैं। नर्तक रंग-बिरंगे परिधान और पगड़ी पहनते हैं। गढ़वाल में छोलिया नृत्य के भांति ही सरौं में तलवार और ढाल की सहायता से किया जाता है। सरौं नृत्य मुख्य रूप से टिहरी व उत्तरकाशी में प्रसिद्ध है।
पौणा नृत्य - भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा शादी विवाह के अवसर पर किए जाने वाला पोणा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है।
5. थड़िया नृत्य
थड़िया थाड़ शब्द से बना है गढ़वाली भाषा में थाड़ का अर्थ होता है आंगन या चौका । थड़िया नृत्य गढ़वाल में बसंत पंचमी के समय विवाहित लड़कियां पहली बार मायके आने पर करती हैं
6. पांडव नृत्य
पांडव नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित है और महाभारत के पांडवों की कहानियों पर आधारित है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का नृत्य है। नर्तक पांडवों और द्रौपदी जैसे पात्रों का अभिनय करते हैं, और इसे नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
7. जागर
जागर उत्तराखंड का एक आध्यात्मिक नृत्य-संगीत रूप है, जिसमें स्थानीय देवी-देवताओं और आत्माओं को आह्वान किया जाता है। यह गीत और नृत्य का मिश्रण है।
विशेषता: जागर में ढोल और हुड़का का उपयोग होता है, और इसे शमशान घाटों या मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता है।
अवसर: धार्मिक अनुष्ठान और पूजा।
8. चौंफला नृत्य
यह नृत्य गढ़वाल में किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता है कि पुरुष नृत्य को चौफुला व स्त्री नृत्य को चौफुलों कहा जाता है। यह एक प्रकार का श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है जो कि असम के बिहू व गुजरात के गरबा नृत्य के समान है।
9. मण्डाण नृत्य
इस नृत्य को केदार नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र के टिहरी एवं उत्तरकाशी में देवी देवता के पूजन देव, और शादी-ब्याह के मौके पर किया जाता है।
10. भैला - भैला नृत्य
गढ़वाल क्षेत्र में यह नृत्य दीपावली के दिन भैला बांधकर किया जाता है।
11. रणभूत नृत्य
गढ़वाल क्षेत्र में वीरगति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर किया जाता है और उनकी आत्माओं की शांति के लिए उसे परिवार के लोग रणभूत नृत्य करते हैं
12. हारुल नृत्य
जौनसारी जनजाति पांडवों को अपना वंशज मानती है। और वह पांडवों के जीवन पर आधारित
हारूल नृत्य करती है। इस नृत्य में 'रमतुला नामक वाद्य यंत्र अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा जौनसारी समाज में जन्मोत्सव शादी विवाह एवं हर्षोल्लास के अवसर पर बुड़ियात लोक नृत्य किया जाता है।
13. खेल
खेल लोक गायन व लोकनृत्य अभिनय की एक विशेष शैली है, इसमें प्रायः राजपूत वर्ग के लोग अधिक भाग लेते है। खेलों में गायन के साथ एक विशेष भंगिया के साथ पद चालन भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में खेल बालक के जन्म उत्सवों, देव उत्सवों में अधिक मनाया जाता है।
लोकगीत एवं लोक नृत्य का सांस्कृतिक महत्व
- सामाजिक एकता : झोड़ा और चांचरी जैसे नृत्य सामुदायिक एकता को बढ़ावा देते हैं।
- आध्यात्मिकता : जागर और पवाड़ा जैसे गीत और नृत्य धार्मिक और ऐतिहासिक भावनाओं को व्यक्त करते हैं।
- प्रकृति से जुड़ाव : न्योली और बंजारा गीतों में पहाड़ों, नदियों, और जंगलों की सुंदरता का वर्णन होता है।
- परंपरा का संरक्षण : ये कला रूप पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, जिससे सांस्कृतिक विरासत जीवित रहती है।
आधुनिक संदर्भ में स्थिति
आजकल, उत्तराखंड के लोकगीत और नृत्य सांस्कृतिक समारोहों, पर्यटन उत्सवों, और मंच प्रदर्शनों के माध्यम से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि, शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण इन पारंपरिक कला रूपों को संरक्षित करने की चुनौती भी है। उत्तराखंड सरकार और सांस्कृतिक संगठन इनके प्रचार-प्रसार के लिए मेले और कार्यशालाएँ आयोजित करते हैं।
Related posts :-

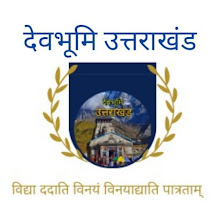

टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubts.
Please let me now.